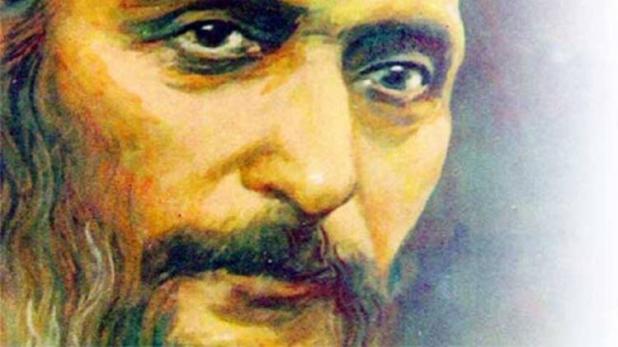- मिथिलेश कुमार सिंह
 ‘मैंने ‘निराला’ की मौत देखी है/ भवानी प्रसाद मिश्र को देखा है गीत बेचते/ अब मैं कविताएं नहीं लिखूंगा।’ दशकों पहले यह कविता नजर से गुजरी थी। अब याद नहीं आ रहा कि कवि कौन है? इतना डरपोक? इतना दब्बू कि कविताएं ही नहीं लिखेगा- सिर्फ इसलिए कि लिखना घाटे का काम है और कि उसमें बड़ा फजीता है, बड़ा छिछियाना पड़ता है!! गोल गैंग न हो तो रोज मरना भी पड़ सकता है, सिर्फ इसलिए? तब ऐसी कविताएं भी अच्छी लग जाया करती थीं, जिन पर अब हंसी आती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि लिखना वाकई रिस्की है और अगर आप जग जीतने यानी हरेक को खुश करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, तब तो इतना रिस्की कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौसम खराब है।
‘मैंने ‘निराला’ की मौत देखी है/ भवानी प्रसाद मिश्र को देखा है गीत बेचते/ अब मैं कविताएं नहीं लिखूंगा।’ दशकों पहले यह कविता नजर से गुजरी थी। अब याद नहीं आ रहा कि कवि कौन है? इतना डरपोक? इतना दब्बू कि कविताएं ही नहीं लिखेगा- सिर्फ इसलिए कि लिखना घाटे का काम है और कि उसमें बड़ा फजीता है, बड़ा छिछियाना पड़ता है!! गोल गैंग न हो तो रोज मरना भी पड़ सकता है, सिर्फ इसलिए? तब ऐसी कविताएं भी अच्छी लग जाया करती थीं, जिन पर अब हंसी आती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि लिखना वाकई रिस्की है और अगर आप जग जीतने यानी हरेक को खुश करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, तब तो इतना रिस्की कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौसम खराब है।
आपके चारों ओर जो हवाएं चल रही हैं, उन पर एतबार मत कीजिएगा और उन चेहरों पर तो हरगिज नहीं जो दीन-दुनिया से आपको खबरदार तो करते हैं, लेकिन बचते-बचाते। दिक्कत यह है कि साहित्य की दुनिया बचने-बचाने की हुआ भी नहीं करती है। बचे तो गये काम से। लेकिन इन्हीं नीम अंधेरों से, इन्हीं तंग सिम्तों से फूटती हैं उम्मीद की नयी कोंपलें भी। दुश्वारियां हैं और बेशक हैं, लेकिन लिखा-पढ़ा ही बचाएगा, चाहे जीते जी सागर सिद्दीकी की तरह आपको भीख ही क्यों न मांगनी पड़े और लोग आपके गुजर जाने को छींक या जम्हाई आने से ज्यादा तवज्जो भले ही न दें।
यह भी पढ़ेंः कन्हैया कुमार ने की आन लाइन चंदे की अपील, खाते में आये 30 लाख
अब सागर सिद्दीकी पर। नाम सुना है कभी आपने इस शख्स का? शायद ही सुना हो। तो सुन लीजिए, यह उस शख्स का नाम है, जिसने ‘दमादम मस्त कलंदर’ जैसी कव्वाली अदबी दुनिया को दी। यह वह कव्वाली है जिसे सुनते-पढ़ते हुए आप भूल जाते हैं कि झूलेलाल सिंधियों के गणदेवता हैं कि हिंदुओं या मुसलमानों के। यह कव्वाली सुनते हुए दीवारें मिट जाती हैं- वे नकली दीवारें, जो बड़ी मशक्कत से बहेलिये के जाल की शक्ल में हमारे-आपके चतुर्दिक बुनी गयी हैं और इन्हें बुनने में सदियां लगीं।
यह भी पढ़ेंः मलिकाइन के पाती- ठांव गुने काजर, कुठांव गुने कारिख
सागर सिद्दीकी मूल रूप से अंबाला के थे, जो देश विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गये। लाहौर उनका ठिकाना बना। घर? उनके पास लाहौर में अपना कोई घर नहीं था। रहा भी होगा तो कब बिक गया, इसकी तफसील कहीं नहीं मिलती। किसी किताब में नहीं, किसी रिसाले में नहीं। उन्हें गजलें कहने के अलावा कोई और कोई काम भी तो नहीं आता था। गजलें खूब कहते थे, ग़ज़लें बेच भी देते थे- जिसे जी में आए खरीद ले और अपने नाम से शाया करा ले।
यह भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गये राष्ट्र को संबोधित कर, होगी जांच
देश विभाजन के बाद खुद को जीवित रखने के लिए उन्हें यतीमखाने या फिर सड़कों की पनाह लेनी पड़ी, भीख मांगनी पड़ी, जहालत झेलनी पड़ी और मनुष्यत्व की गरिमा को नीचे गिराने वाले सारे काम (चोरी-चकारी या खून-खच्चर को छोड़ कर) करने पड़े। बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह कव्वाली सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्म ‘लाल मिर्जा’ में बीती सदी की पांचवीं दहाई में आई और इसे गाया नूरजहां ने, जो बाद में मल्लिकाए तरन्नुम कहलाईं। 1974 में साग़र का इंतकाल हो गया किसी फुटपाथ किनारे। लेकिन यह तस्वीर का बहुत मामूली सा टुकड़ा है।
यह भी पढ़ेंः गरीबों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं राहुल गांधीः सुशील मोदी
इतने छोटे फ्रेम में यह शायर आएगा भी नहीं। खैर। साग़र की जो गजलें दो-दो, चार-चार रुपये तक में बिकने से रह गयीं, वे भी भरोसा जगाती हैं कि राह चाहे जितनी भी मुश्किल हो, वह आदमीयत के हमवार होगी, उसे होना ही है हमवार- वक्त चाहे जो लगे। इस कव्वाली की धुन बनाई थी आशिक हुसैन ने और साग़र की तरह आशिक को भी पेट भरने के लिए पकौड़े और चाट और पानी पूरी के ठेले लगाने पड़े या ठेलों पर काम करना पड़ा, क्योंकि वक्त के साथ उनकी धुन के कद्रदान नहीं रह गये थे। उनकी भी मौत वैसी ही मुफलिसी और गुमनामी में हुई।
यह भी पढ़ेंः बिहार की हाट सीट पटना साहिब, दरभंगा व बेगूसराय बन गयीं हैं
यह तो हुआ साग़र सिद्दीकी को जानने का बहुत सपाट और सतही नुस्खा। अब रुख करें उनकी शायरी पर और उनकी एक ग़ज़ल के कुछ शेर पर गौर फरमाएं:
चराग़-ए-तूर जलाओ बड़ा अँधेरा है। ज़रा नक़ाब उठाओ बड़ा अँधेरा है।।
अभी तो सुब्ह के माथे का रंग काला है। अभी फ़रेब न खाओ बड़ा अँधेरा है।।
वो जिन के होते हैं ख़ुर्शीद आस्तीनों में। उन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अँधेरा है।।
मुझे तुम्हारी निगाहों पे ए’तिमाद नहीं। मिरे क़रीब न आओ बड़ा अँधेरा है।।
फ़राज़-ए-अर्श से टूटा हुआ कोई तारा। कहीं से ढूँड के लाओ बड़ा अँधेरा है।।
बसीरतों पे उजालों का ख़ौफ़ तारी है। मुझे यक़ीन दिलाओ बड़ा अँधेरा है।।
जिसे ज़बान-ए-ख़िरद में शराब कहते हैं। वो रौशनी सी पिलाओ बड़ा अँधेरा है।।
यह ग़ज़ल पढ़ते हुए आपको वह धारा याद नहीं आती, जो ग़ालिब से शुरू होती है और फ़िराक़ तक जाती है? वह अकुलाहट नजर नहीं आती कि किसी भी तरह रोशनी तो आए, चाहे जहां से भी हो और जैसे भी हो? अंधेरे के खिलाफ (अंधेरे से ज्यादा अंधेरगर्दी के खिलाफ) गवाही देने वाले ऐसे कितने अदीबों को हम याद रखते हैं? जाओ …कवि जाओ, तुम्हारा यही हश्र बदा था। शुक्र मनाओ कि तुम पागल नहीं हुए, कोड़े नहीं खाये। लोग तुम्हें पढ़ेंगे, भरोसा रखना। आज नहीं तो कल। शुक्र मनाओ कि ग़ज़लें बेचते रहने की गंभीर लाचारी के बावजूद तुमने लिखने से कभी तौबा नहीं की। कसम नहीं खायी कि अब नहीं लिखना।
यह भी पढ़ेंः बिहार दिवस पर विशेषः बिहार के निर्माता को भूलती नई पीढ़ी